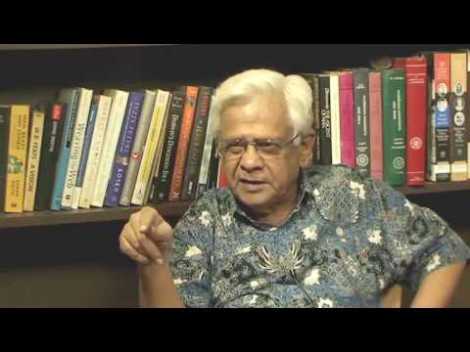‘प्रतिमान’ के आगामी अंक के लिए लिखा गया
28 जुलाई के महाराष्ट्र टाईम्स में प्रकाशित एक अलग किस्म के लेख पर अचानक निगाह गयी थी जिसका शीर्षक था ‘आमचा दादोजी’। प्रस्तावना पढ़ने पर पता चला कि गो पु देशपांडे अर्थात गोविंद पुरूषोत्तम देशपांडे ( जो मराठी भाषिकों के लिए ‘गोपु’ के नाम से तो ‘इकोनोमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली’ जैसी अन्तरराष्ट्रीय ख्याति की पत्रिका के पाठकों के लिए – जहां उन्होंने तीन दशक तक नियमित कॉलम लिखा – जीपीडी के नाम से जाने जाते रहे) की अनुजा ज्योति सुभाष ने अपने दादोजी अर्थात सबसे बड़े भाई के पचहत्तरवे वर्ष पूरे करने पर यह लेख लिखा था। लेख में सातारा जिले के रहमतपुर गांव में बीते गो पु के बचपन की तमाम यादें थीं, जिन्हें कोलाज के रूप में उन्होंने पेश किया था। आजादी के आन्दोलन में शामिल उनके दादाजी और उनके माता पिता, बचपन से ही प्रचण्ड मेधावी के रूप में चर्चित गो पु की भुलक्कडी के तमाम किस्से जो हमेशा सोचने समझने में ही खोए रहते थे, यहां तक कि उन्हें खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता था, इन सभी को उन्होंने बयां किया था. गो पु की पहली विदेश यात्रा के लिए उन्हें बिदा करने गए सभी छोटे भाई बहन किस तरह दुखी होकर हवाई अड्डे पर रो रहे थे, इसका भी जिक्र उन्होंने किया था।
अपनी अनुजा के संस्मरण के बहाने गो पु के जीवन का एक ऐसा अध्याय सामने खुल रहा था, जिसके बारे में शायद ही कहीं लिखा गया हो। लेख पढ़ते हुए किसे इस बात का गुमान हो सकता था कि मैं जिस वक्त उन पंक्तियों को पढ़ रहा था तब मस्तिष्काघात अर्थात ब्रेन हैमरेज के चलते वह अस्पताल में भरती थे और कोमा में चले गए थे। उन्हें इसके बाद कभी होश नहीं आया। पुणे के अपने घर में ही उन्होंने अन्तिम सांस ली।
वैसे बहुत कम लोग होते हैं जिनका गुजर जाना कई दायरों में एक साथ एक सदमे की तरह महसूस किया जाता है, कई दायरों को एक साथ सूना कर देता है , गोपु के गुजर जाने पर यह बात सटीक बैठती है। चीनी भाषा के विद्धान, जवाहरलाल नेहरू विश्ववि़द्यालय में अन्तरराष्ट्रीय मामलों में अध्यापन – जिसमें उनका विशेष फोकस चीन था’ और उन्होंने ‘चायना स्टडी ग्रुप’ की भी स्थापना में योगदान दिया था – ; उध्वस्त धर्मशाला’, अंधार यात्रा, चाणक्य विष्णुगुप्त, रास्ते और सत्यशोधक जैसे नाटकों के लेखक ; इकोनोमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली में नियमित स्तम्भलेखन ; संस्कृत साहित्य से लेकर मराठी साहित्य के गहन अध्येता ; साम्प्रदायिकता के खिलाफ या ऐसे अन्य जनपक्षीय मसले पर दिल्ली की सड़क पर सामूहिक प्रतिरोध में भी समय समय पर उनकी मौजूदगी और सबसे बढ़ कर वामपंथी आन्दोलन के साथ अपनी लम्बे समय की चली आयी संलग्नता। वैसे महाराष्ट्र के बाहर के बहुत कम लोग जानते होंगे कि उन्होंने कविताएं भी लिखी थीं और कुछ समय पहले उनका कवितासंग्रह भी प्रकाशित हुआ था। उनकी जीवनसंगिनी कालिंदी देशपांडे, खुद नारी मुक्ति आन्दोलन की अग्रणी कार्यकर्ती थी, जिनका 2009 में इन्तक़ाल हुआ। एक साथ उन्होंने जिस तरह एक माध्यम से दूसरे माध्यम या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बेहद सहजता के साथ अपनी यात्रा जारी रखी और विचारों की दुनिया में भी एक अलग छाप छोड़ी इसे देखते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए किसी ने ठीक ही लिखा है कि वह भारत के अपने ‘रेनेसां मैन’ (renaissance man) थे।
उनके जीवन में विचारों की प्रधानता की यही वह स्थिति थी जिसके चलते जिन नाटकों की उन्होंने रचना की वहां पर भी एक नयी जमीन तोड़ने में वह सफल रहे। उनके नाटयलेखन ने मराठी रंगमंच में ही नहीं बल्कि भारतीय रंगमंच में एक अलग छाप छोड़ी , जिसे चर्चा की शैली वाला नाटक कहा गया। वह 1973 का किस्सा है जब सत्यदेव दुबे ने नाटयलेखन शिविर का आयोजन किया था, जिसमें सतीश आलेकर से लेकर (बाद में चर्चित) उस वक्त के कई उदितमान नाटककारों ने हिस्सा लिया था। इसी शिविर में गो पु ने अपने नाटक ‘उध्वस्त धर्मशाला’ का पठन किया था। एक विश्वविद्यालय में कार्यरत एक मार्क्सवादी प्रोफेसर को झेलनी पड़ रही घुटन, प्रताडना पर केन्द्रित यह नाटक श्रीराम लागू, को भी बेहद पसन्द आया था, जो खुद उस वक्त़ मराठी नाटयजगत में सफलता की बुलन्दियों पर थे। नाटक के मंचन के लिए उन्होंने कई पेशेवर नाटयसमूहों से सम्पर्क किया मगर कोई तैयार नहीं हुआ। उन सभी को उसमें कोई व्यावसायिक तत्व नहीं दिखाई दिया। बाद में खुद श्रीराम लागू ने ही इस नाटक को अभिनीत किया था। नाटक न केवल चर्चित हुआ बल्कि कई अन्य भाषाओं में अनूदित भी हुआ और उसका मंचन भी हुआ।
उनके एक अन्य नाटक ‘रास्ते’ में भी वही चर्चाशैली अभिव्यक्त होती है। नाटक के केन्द्र में हैं अलग अलग राजनीतिक रूझानों वाले तीन मित्रोंें की – जो बडोदा विश्वविद्यालय से स्नातक पढ़ कर निकलते हैं – जीवनयात्रा। इनमें से एक मित्र मार्क्सवादी विचारों का है, एक संघी है तो तीसरा मस्तमौला किस्म का है। इन मित्रों की जीवनयात्रा के बहाने उन्होंने समसामयिक राजनीतिक सामाजिक घटनाक्रम, आन्दोलन पर अपना नज़रिया पेश करने की कोशिश की थी। नाटक के अन्तिम दृश्य में वह तीनों दोस्त 21 वीं सदी के पुणे में मिलते हैं, जहां फिर उनकी तीखी बहस होती है। उनके साथ उनकी जीवनसंगिनियां भी हैं, जो इस पूरी बहस से निर्लिप्त है। बातचीत के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि समाज में नकारात्मकता फैली है और हमें सम्वाद जारी रखना चाहिए। याद रहे कि नाटक के मार्क्सवादी पात्र की बेटी की नक्सलवादी आन्दोलन में सक्रियता और उसके चित्रण को लेकर गो पु को आलोचना का भी शिकार होना पड़ा था।
वैसे आलोचना का एक वक्त वह भी आया था जब तियेनआनमेन चौक की घटनाएं हुई थीं। बीजिंग के तियेनआनमेन चौक की घटनाओं के बाद (1989) जब छात्रों एवं मजदूरों के एक व्यापक आन्दोलन को चीनी हुकूमत ने बर्बरता के साथ कुचल दिया था और चीन के समाजवादी रास्ते से हटने की चर्चाएं अधिक तेज हुई थीं, उस वक्त भी चीन के अध्येता के तौर पर उन्होंने घटनाओं का ‘वस्तुनिष्ठ विश्लेषण’ पेश किया था, यह भी कहा था कि ऐसी स्थितियां आनेवाले दिनों में भी बन सकती हैं, मगर चीन के इन बदलावों को लेकर आफिशियल मार्क्सिस्ट पोजिशन को प्रश्नांकित नहीं किया था।
‘जननाटय मंच’ के कहने पर उन्होंने महात्मा फुले के जीवन पर आधारित नाटक ‘सत्यशोधक’ की रचना की थी। इस नाटक की प्रस्तुति की एक खासियत यह थी कि पुणे के स्वच्छता विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लेकर इसे तैयार किया गया था, नाटक इस कदर लोकप्रिय हुआ कि एक साल के अन्दर पूरे महाराष्ट्र में उसका सौ स्थानों पर मंचन हुआ।
अगर नाटकों के जरिए उन्होंने विचारों की अपनी मुहिम को एक अलग आयाम दिया तो ‘इकोनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली’ के उनके नियमित स्तंभ के जरिए उसे एक अलग निखार दिया। जब वह लिखते थे तब बेबाक ढंग से लिखते थे। सलमान रश्दी के मसले पर बहुत मुखर होकर बोलनेवाले और शिवसेना द्वारा रोहिग्टन मिस्त्री की किताब पर लगायी गयी ‘पाबन्दी’ पर अचानक मौन होने वाले भारत के लिबरल/उदारवादी के दोहरेपन को उजागर करने में न उन्होंने संकोच किया (सिलेक्टिव रिस्पान्सेस) और न ही किताबों या अन्य रचनाओं के साथ सीधी बौद्धिक अन्तर्क्रिया करने के बजाय उस पर पाबन्दी लगाने या तोडफोड का सहारा लेने की भारतीय प्रवृत्ति को बख्शा (प्राइड एण्ड प्रेजुडिस इन मराठा कन्ट्री) इन्हीं में से कुछ लेखों का संकलन 2009 में आया था जिसका शीर्षक था ‘टाकिंग द पोलिटिकल कल्चरली’। इस संकलन में वामपंथी कार्यकर्ता होने का स्वर प्रधान दिखता है। प्रस्तुत किताब की समीक्षा करते हुए ईपीडब्लू के अपने आलेख में अनिकेत आलम लिखते हैं कि इसका पहला निबंध एक तरह से दक्षिण एशिया की बौद्धिक परम्पराओं के प्रति वाम कार्यकर्ताओं की अनभिज्ञता के खतरनाक परिणामों को लेकर उन्हीं से एक सम्वाद है।
इसी किताब में एक स्थान पर गोपु लिखते हैं:
प्रगतिशील आन्दोलन में अपने बौद्धिक पुरखों के प्रति कोई उत्साह नहीं दिखता..ऐसा प्रतीत हो सकता है कि प्रगतिशील सांस्कृतिक आन्दोलन के लिए दुनिया के गैरउच्चवर्णीय जनों से निकले फुले और नारायणगुरूओं की कोई अहमियत न हो ..(इसके अलावा) यह दिख सकता है कि प्रगतिशील सांस्कृतिक आन्दोलन ने कभी क्लासिकीय भाषाओं के साथ अपने रिश्ते को परिभाषित नहीं किया। जनता की जुबां के सेलिब्रेशन का मतलब क्लासिकीय को खारिज करना हो, यह कोई जरूरी नहीं है।..इसके चलते कई लोग संस्कृत जैसी भाषा को किसी जाति समूह या धार्मिक समूह तक सीमित कर देते हैं। यह वही हुआ कि आप उर्दू को मुसलमानों तक सीमित कर दें।..
(प्रगतिशील सांस्कृतिक आन्दोलन) क्लासिकीय और जन/फोक के नितान्त अनैतिहासिक, दरअसल पूरी तरह झूठे अन्तर्विरोध में संतृप्त दिखता है ..वह एक तरह से , क्लासिसिजम और क्लासिकीय परम्परा को रूढिवाद को सौंपने के लिए आंशिक तौर पर जिम्मेदार है।
अपनी किताब ‘वर्ल्ड आफ आयडियाज इन माडर्न मराठी’ (तूलिका, 2009) में वह आधुनिक भारत के बौद्धिक इतिहास पर निगाह डालते हैं, जिसमें वह फुले, विनोबा भावे और सावरकर के विचारों की चर्चा के बहाने एक अलग किस्म का बौद्धिक हस्तक्षेप करते हैं। जीपीडी के मुताबिक भारत में 19 वीं सदी के इतिहासलेखन की समस्या यह है कि वह इस बिन्दु से प्रस्थान करती है कि ‘‘भारत एक इतिहास क्षेत्र है।’’ अपनी प्रस्तावना में वह सचेत तौर पर एक स्वायत्त होने के नाते तथा साथ ही साथ भारतीय राष्ट्र का हिस्सा होने के तौर पर क्षेत्र को आगे रखते हैं। यूरोप के साथ सादृश्यता दिखाते हुए वह कहते हैं कि जबकि जर्मन आधुनिकता व्यापक यूरोपीय आधुनिकता का ही हिस्सा है, मगर जब तक आप जर्मन चिन्तन के इतिहास से परिचित न हों तब तक आप उसका अध्ययन नहीं कर सकते है। उनके मुताबिक ‘‘भारत में इतिहास को बहुवचनी होना चाहिए। भारत का इतिहास उसकी राष्ट्रीयताओं का इतिहास है।’ प्रस्तुत किताब की चर्चा करते हुए ईपीडब्लू के उसी आलेख में अनिकेत आलम जोड़ते हैं कि इसका मतलब यह नहीं निकाला जा सकता कि ‘गोपु किसी ‘‘देशज’ (indigenist or nativist) पोजिशन की हिमायत करते हैं और वह आधुनिकता की किसी उत्तर आधुनिक आलोचना से प्रभावित है जो इतिहास के महाख्यान के बरअक्स स्थानीय को सेलिब्रेट करती है। दरअसल वह ऐसा बौद्धिक रूख अख्तियार करते हैं जो इन सिद्धान्तों और रचनाओं के प्रति स्थूल रूप से दूरी रखता हो, इसके लिए जिन बौद्धिक उपकरणों का वह इस्तेमाल करते हैं वह क्लासिकीय वाम-उदारवादी अकादमिक जगत के दृष्टिकोण से नजदीक दिखती है- जो मार्क्सवाद, यथार्थवाद और साम्राज्यवाद विरोध से प्रेरित है तथा सशक्त मानवतावादी पोजिशन्स में स्थापित है।’
भारत के वामपंथ की इस वक्त अन्तर्विरोधी छवि नज़र आती है। दुनिया के अन्य हिस्सों के विभिन्न वाम संगठनों/आन्दोलनों के बरअक्स जिन्हें सोविएत विघटन के बाद हारों या शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसके लिए यह मुमकिन हुआ है कि वह अपने आप को बनाए रखे और कुछ स्थानों पर विस्तारित भी हो। अपना अस्तित्व बचाये रखने या तमाम चुनौतियों के बीच अपनी निरन्तरता कायम रखने का अर्थ यह नहीं है कि उसके सामने चुनौतियां नहीं हैं। इक्कीसवीं सदी में सामाजिक बदलाव की मुक्तिकामी दृष्टि/विजन पेश करने का, जनता की लामबन्दी के लिए नयी किस्म की रणनीतियां विकसित करने का और सांगठनिक तौर पर अपने आप को पुनर्जीवित करने का सवाल उसके सामने आज भी बना हुआ है। दलित मुक्ति का प्रश्न या जाति के विनाश के लिए समग्र संघर्ष का सवाल ऐसा ही एक अहम सवाल है, जिस पर गम्भीरता से ध्यान देने की जरूरत है।
‘सिलेक्टेड रायटिंग्ज आफ जोतिराव फुले’ की प्रस्तावना में गो पु जोतिराव फुले के आकलन के बहाने इन प्रश्नों को लेकर प्रचलित वाम समझदारी से एक अलग रेखा खींचते दिखते हैं। मालूम हो कि फुले ने सामाजिक मुक्ति के क्षेत्र में एक रैडिकल प्रवाह के विकास में अहम भूमिका अदा की थी जिन्होंने ‘शेटजी और भटजी’ (महाजन और ब्राह्मण) से मुक्ति की बात रेखांकित की थी। फुले की अगुआई में संचालित यही आन्दोलन था जिसने भारतीय सन्दर्भ में जिस स्त्री मुक्ति की बात कही वह विचार उंची जाति से सम्बद्ध समाज सुधारकों से गुणात्मक तौर पर अलग था। फुले द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज के अग्रणी लोखंडे ही थे जिन्होंने 19 वीं सदी के उत्तरार्द्ध में बम्बई के कामगारों को संगठित कर उनकी पहली यूनियन की नींव डाली थी।
गोपु लिखते हैं:
‘फुले का फ़लक व्यापक था, उनका प्रसार विशाल था। उन्होंने अपने वक्त़ के अधिकतर महत्वपूर्ण प्रश्नों – धर्म, वर्णव्यवस्था, कर्मकाण्ड, भाषा, साहित्य, ब्रिटिश हुकूमत, मिथक, जेण्डर प्रश्न, कृषि में उत्पादन की परिस्थितियां, किसानों की हालत आदि – को चिन्हित किया और उनको सैद्धान्तिक शक्ल देने की कोशिश की.। इस सूची को और बढ़ाया जा सकता है । 19 वीं सदी के भारत में ऐसी कोई दूसरी शख्सियत नज़र नहीं आती, जिनके सरोकार इतने व्यापक हों।.. क्या फुले को फिर समाज सुधारक कहा जा सकता है ? इस जवाब होगा ‘नहीं’। एक समाज सुधारक उदार मानवतावादी होता है और फुले क्रान्तिकारी अधिक थे। उनके पास विचारों की समग्र प्रणाली थी, और वह उन प्रारम्भिक विचारकों में से थे, जिन्होंने भारतीय समाज मे वर्गो की पहचान की थी। उन्होंने भारतीय समाज के द्वैवर्णिक संरचना का विश्लेषण किया था, और सामाजिक क्रान्ति के लिए शूद्रों-अतिशूद्रों को अग्रणी कारकशक्ति/एजेंसी के तौर पर चिन्हित किया था। (पेज 20, लेफ्टवर्ड)
किताब की प्रस्तावना के अन्त में वह मार्क्स के योगदान के साथ फुले के योगदान की तुलना करते लिखते हैं:
‘अपने आलेख ‘ब्रिटिश रूल इन इंडिया’ में मार्क्स बताते हैं कि इंग्लण्ड के आगमन ने किस तरह भारतीय जनता की ‘मौजूदा दुर्गति को एक खास किस्म की विषण्णता प्रदान की। भारत के किसान समुदाय की इस दुर्गति और विषण्णता के प्रति फुले का भी सरोकार था। और मार्क्स की तरह, फुले का जीवन इस विषण्णता के विश्लेषण में सन्नद्ध रहा ताकि इसमें से कोई रास्ता निकाला जा सके। दूसरे शब्दों में कहें तो विचारों की एक प्रणाली तब तक पूरी नहीं कही जा सकती जब तक उसमें उम्मीद का तत्व न हो। मार्क्स ने उस काम को अंजाम दिया। फुले ने भी किया। उसे अमली जामा पहनाना हमारी जिम्मेदारी है।